शूद्र
शूद्र
| |
| विवरण | शूद्र भारतीय समाज व्यवस्था में चतुर्थ वर्ण या जाति है। |
| उत्पत्ति | शूद्र शब्द मूलत: विदेशी है और संभवत: एक पराजित अनार्य जाति का मूल नाम था। |
| पौराणिक संदर्भ | वायु पुराण का कथन है कि शोक करके द्रवित होने वाले परिचर्यारत व्यक्ति शूद्र हैं। भविष्यपुराण में श्रुति की द्रुति (अवशिष्टांश) प्राप्त करने वाले शूद्र कहलाए।[1] |
| वैदिक परंपरा | अथर्ववेद में कल्याणी वाक (वेद) का श्रवण शूद्रों को विहित था।[2] परंपरा है कि ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महीदास इतरा (शूद्र) का पुत्र था। किंतु बाद में वेदाध्ययन का अधिकार शूद्रों से ले लिया गया। |
| ऐतिहासिक संदर्भ | शूद्र जनजाति का उल्लेख डायोडोरस, टॉल्मी और ह्वेन त्सांग भी करते हैं। |
| आर्थिक स्थिति | उत्तर वैदिक काल में शूद्र की स्थिति दास की थी अथवा नहीं[3] इस विषय में निश्चित नहीं कहा जा सकता। वह कर्मकार और परिचर्या करने वाला वर्ग था। |
| मध्य काल | कबीर, रैदास, पीपा इस काल के प्रसिद्ध शूद्र संत हैं। असम के शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित मत, पंजाब का सिक्ख संप्रदाय और महाराष्ट्र के बारकरी संप्रदाय ने शूद्र महत्त्व धार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया। |
| आधुनिक काल | वेबर, भीमराव आम्बेडकर, ज़िमर और रामशरण शर्मा क्रमश: शूद्रों को मूलत: भारतवर्ष में प्रथमागत आर्यस्कंध, क्षत्रिय, ब्राहुई भाषी और आभीर संबद्ध मानते हैं। |
| संबंधित लेख | वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, चर्मकार, मीणा, कुम्हार, दास, भील, बंजारा |
| अन्य जानकारी | पद से उत्पन्न होने के कारण पदपरिचर्या शूद्रों का विशिष्ट व्यवसाय है। द्विजों के साथ आसन, शयन वाक और पथ में समता की इच्छा रखने वाला शूद्र दंड्य है।[4] |
शूद्र भारतीय समाज व्यवस्था में चतुर्थ वर्ण या जाति है। वायु पुराण[5], वेदांतसूत्र[6] और छांदोग्य एवं वेदांतसूत्र के शांकरभाष्य में शुच और द्रु धातुओं से शूद्र शब्द व्युत्पन्न किया गया। वायु पुराण का कथन है कि शोक करके द्रवित होने वाले परिचर्यारत व्यक्ति शूद्र हैं। भविष्यपुराण में श्रुति की द्रुति (अवशिष्टांश) प्राप्त करने वाले शूद्र कहलाए।[7] दीर्घनिकाय में खुद्दाचार (क्षुद्राचार) में सुद्द शब्द संबद्ध किया गया।[8] होमर के द्वारा उल्लिखित 'कूद्रों' से शूद्र शब्द जोड़ने का भी प्रयत्न हुआ।[9]
उत्पत्ति
शूद्र शब्द मूलत: विदेशी है और संभवत: एक पराजित अनार्य जाति का मूल नाम था। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है और प्रयत्न और विकास से अन्य वर्ण अवस्थाओं में पहुँचता है। वास्तव में प्रत्येक में चारों वर्ण स्थापित हैं।
पारंपरिक संभावनाएँ
ऋग्वेद के पुरुषसूक्त[10] से पुरुष के पदों से शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है। पुरुषोत्पत्ति का यह सिद्धांत ब्राह्मण ग्रंथ[11], वाजसनेयी संहिता[12], महाभारत[13], पुराण[14] में शूद्रदेव पूषा से शूद्र की उत्पत्ति बतलाई गई है। विष्णु और वायु पुराण के अनुसार यज्ञनिष्पत्ति के लिए चतुर्वर्णों का सर्जन हुआ। शांतिपर्व और गीता में गुणकर्म के आधार पर चातुर्वर्ण्य प्रतिष्ठित है। हिंसा, अनृत, लोभ और अशुचिता के कारण तामसी द्विज कृष्ण होकर शूद्र वर्ण में परिणत हुए।[15] बौद्ध परंपरा में बंधपादपच्य से इव्य (सेवक) और किन्ह (कृष्ण) निकले।[16] जैन परंपरा में तीर्थंकर ऋषभदेव और उनके शिष्य भरत ने चारों वर्णों का निर्माण किया।[17]
ऐतिहासिक पर्यालोचन
पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार प्रारंभ में दो ही वर्ण थे, आर्य और दास।[18] अथर्ववेद में आर्य दास का युग्म आर्यशूद्र में परिणत हो गया।[19] अत: शूद्र दास दस्यु के उत्तराधिकारी हैं। किंतु यह मत निर्भ्रांत नहीं। उपर्युक्त स्थलों पर[20] शब्द आर्य नहीं किंतु अर्य (वैश्य) है। वेबर, भीमराव आम्बेडकर, ज़िमर और रामशरण शर्मा क्रमश: शूद्रों को मूलत: भारतवर्ष में प्रथमागत आर्यस्कंध, क्षत्रिय, ब्राहुई भाषी और आभीर संबद्ध मानते हैं। शूद्र जनजाति का उल्लेख डायोडोरस, टॉल्मी, और ह्वेनसांग भी करता है। शूद्र वर्ण में संभवत: आर्य और अनार्य कर्मकरों के युगल तत्व थे।
पाणिनि का उल्लेख
पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है- एक अनिरवसित, जो हिंदू समाज के अंग थे, और दूसरे निरवसित (शूद्राणामनिरवसितानाम्)।[21] इस सूत्र पर पतंजलि का विशद भाष्य शूद्रों की शुंगकालीन स्थिति का परिचायक है। 'अनिरवसित शूद्र वे हैं, जो आर्यावर्त की भौगोलिक सीमा के भीतर रहते हैं। इसके विपरीत पतंजलि ने आर्यावर्त की सीमा के बाहर के शूद्रों में कुछ विदेशियों का उल्लेख किया है, जैसे शक और यवन। पतंजलि के समय की ऐतिहासिक स्थिति में शक लोग ईरान और अफ़ग़ानिस्तान की सीमा पर शकस्थान में जमे थे और यवन अर्थात यूनानी लोग बाल्हीक और गंधार में प्रतिष्ठित थे। इसी सूत्र पर पतंजलि का दूसरा उदाहरण 'किष्किंधगब्दिकं' है। पाणिनि के सिंध्वादि-गण [22] में किष्किन्धा और गब्दिका दोनों का पाठ है। किष्किन्धा गोरखपुर ज़िले का खुखुंदो और गब्दिका चंबा का गद्दी प्रदेश था। ये दोनों उस समय आर्यावर्त की सीमा से बाहर माने जाते थे।
मौर्य साम्राज्य की कमर टूटने पर विदेशियों के धक्के से आर्यावर्त की सीमाएँ यहाँ तक सिकुड़ गई कि घर के दुआरे पर स्थित किष्किन्धा गब्दिका भी बाहर गिने जाने लगे। पंतजलि के अनुसार मृतप, चांडाल आदि निम्न शूद्र जातियाँ प्राय: ग्राम, घोष, नगर आदि आर्य बस्तियों में घर बनाकर रहती थीं। पर जहाँ गांव और शहर बहुत बड़े थे, वहाँ उनके भीतर भी वे अपने मुहल्लों में रहने लगे थे। ये समाज में सबसे नीची कोटि के शूद्र थे। इनसे ऊपर बढ़ई, लोहार, बुनकर, धोबी, तक्षा, अयस्कार, तंतुवाय, रजक आदि जातियों की गणना भी शूद्रों में थी। वे यज्ञ से सम्बंधी कुछ कार्यों में सम्मिलित हो सकते थे, पर उनके साथ खाने के बर्तनों की छुआछूत बरती जाती थी। इनमें भी ऊँची कोटि के शूद्र वे थे, जो आर्यों के घर का न्यौता होने पर उन्हीं बर्तनों में खा-पी सकते थे, जिनमें कि घर के लोग खाते-पीते थे। वस्तुत: आर्य और शूद्र की समस्या आर्य एवं मुंडा निषाद-शबर आदि जातियों को एक सामाजिक तंत्र के अंर्तगत लाने की समस्या थी। दूसरी ओर शक-यवन सदृश विदेशी शूद्रों को भी भारतीय समाज में स्थान देने की समस्या थी।[23] मालवपुत्र ही वर्तमान 'मलोत्रे' हो सकते हैं।[24]
धार्मिक स्थिति
विविध युगों और परंपराओं में शूद्रों की स्थिति विभिन्न थी।
वैदिक परंपरा
यज्ञ आधान के अधिकारी न होते हुए लियाज्ञिक समारोह में सम्मिलित हो सकते थे। पुरुषमेध के प्रसंग में[25] वे त्रैवर्णिकों के साथ वर्णित हैं। राजसूय में दानप्राप्ति[26] और सोमपान[27] करते थे। हविष्कृत में आधान से आहूत होते थे और महाव्रत में उनका अपना कार्य था।
- अथर्ववेद
अथर्ववेद[28] में कल्याणी वाक (वेद) का श्रवण शूद्रों को विहित था। बृहद्देवता[29] और पंचविंश ब्राह्मण[30] से दासीपुत्र कक्षीवत, पंचविंश[31] से शूद्रोत्पन्न वत्स, छांदोग्य से सत्यकाम जाबाल तथा शूद्रराजा रैक्व के वेद विद्या का अध्ययन ज्ञात होता है। दासीपुत्र कवष ऐलूष ऋग्वेद[32] के ऋषि के रूप में विख्यात है। परंपरा है कि ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महीदास इतरा (शूद्र) का पुत्र था। किंतु बाद में वेदाध्ययन का अधिकार शूद्रों से ले लिया गया। गौतम धर्मसूत्र[33] में वैदिक श्रवण, उदाहरण और धारण करने पर शूद्र को दंडार्ह माना गया।
बौद्ध
अश्वघोष की वज्रसूची[34] का कथन है कि "दृश्यत च शूद्रा अपि क्वचिद् वेदव्याकरण - सर्वशास्त्रविद:।" शार्दूलकर्णावदान में चांडाल त्रिशुंक सांगोपांग वेद, उपनिषद का ज्ञाता है। उद्दालक जातक में शूद्र भी श्रुति का अध्ययन और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं :-
खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुद्दा चण्डाल पुक्कसा। सव्वे वा सोरता दांता सव्वे वा परिनिव्वुता।।
जैन
'उत्राध्ययन सूत्र'[35] का चांडाल हरिकेशी, उवासगदसाओ[36] का सद्दाल कुंहार, और 'अंतगडदसाओ' का मालाकार अर्जुन निम्नवर्ण होकर भी आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त कर सके। अनवद्य आचार और उपस्कार की शुचिता होने पर शूद्र भी देवपूजन देवकार्य के योग्य माना जाता था।[37] किंतु शूद्र श्रावक हो सकता है मुनि नहीं।[38] इसी प्रकार शूद्र पूजकाचार्य नहीं हो सकता।[39]
आगम (शैव)
आगम (शैव) संप्रदायों में कुछ, यथा शैव सिद्धांत संप्रदाय तथा पाशुपत, वर्णभेद को स्वीकार करते हैं। पाशुपतसूत्र में 'शूद्रेण नाभिभाषेच्च' का विधान है किंतु पंचतंत्र में पाशुपत तपस्वी के वर्णन में कहा है कि शूद्र अथवा चांडाल भी दीक्षित होने पर भस्मांग - शिवस्वरूप हो जाता है। कौल[40] तो यह मानते हैं कि 'भैरवीचक्र में प्रविष्ट होने पर शूद्र भी द्विजाति हो जाता है।' स्वच्छंदतंत्र दीक्षा के पश्चात् शूद्र को उपवीत धारण करने की व्यवस्था करता है।[41]
- वैष्णवी दीक्षा
(वैष्णव) वैष्णवी दीक्षा सारे वर्णों को विहित है। किंतु दीक्षोपरांत भी वर्णभेद की स्थिति रहती है। यथा नामसंस्कार में चारों वर्णों का नामांत क्रमश: शर्मा, वर्मा, गुप्त और दास[42] होना चाहिए, पंजगव्य क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र[43] को देना चाहिए। शूद्र का उपवीत गुणमंत्र[44] से युक्त होता है, कवचमंत्र[45] से नहीं। शूद्रों के लिए अनिरुद्ध विशेष रूप से पूज्य है। पांचरात्र में कुछ शूद्र भक्त हुए जो संप्रदाय में विशेष प्रतिष्ठित हो सके। आंबाल देवदासी का नाम विशेष विख्यात है।
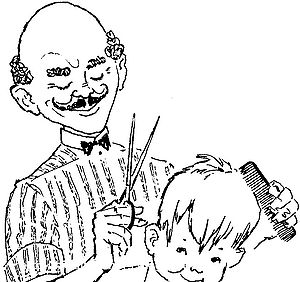
पुराण
अनेक अमंत्रक संस्कार शूद्रों को विहित हैं। साधारण वृद्धि श्राद्ध, पंचमहायज्ञ, वृषोत्सर्ग तथा संपूर्ण पूर्त कर्म एवं पुराण, महाभारत श्रवण शूद्र कर सकते हैं। आर्ष क्रम से शूद्र कश्यपगोत्रीय और बाजसनेय शाखा के हैं। पुराणों की स्मार्त वैष्णव और स्मार्त शैव परंपरा के शूद्रों को भी क्रमश: गोपीचंदन, तुलसी और ऊध्वंपुंड्र[46] तथा भस्मयुक्त पुंड्र एव रुद्राक्ष माला का विधान है।[47]
महाभारत
शांतिपर्व[48] पाकयज्ञ और पूर्ण पात्र दक्षिणा का विधान शूद्रों के लिए करता है। शूद्र पैजवन ने ऐंद्राग्न यज्ञ किया था।
शूद्रो पैजवनो नाम सहस्राणां शतं ददौ।
ऐद्राग्नेन विधानेन दक्षिणाभिति न:श्रुतम्।।[49]
मध्ययुग
स्मार्त परंपरा के तुलसीदास शूद्र को 'ताड़नीय' और 'विप्र अवमानी शूद्र' को शोचनीय मानते हुए भक्त शूद्र को 'भुवन भूषण' भी मानते हैं। उन्हें शूद्रों के द्वारा उपवीत धारण कर व्यासपीठ पर आसीन हो द्विजों को उपदेश देना आलोचनीय लगता है।[50] वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य कृष्णदास शूद्र होते हुए भी संप्रदाय में विशेष सम्मानित थे। छीतस्वामी के विट्ठल के विषय में कहा कि "अवकें स्त्रीसूद्रादिक सबकां ब्रह्म संबंध करावे।" निर्गुनियाँ और संत संप्रदाय में जातिभेद मान्य नहीं था। कबीर, रैदास, सेना, पीपा इस काल के प्रसिद्ध शूद्र संत हैं। असम के शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित मत, पंजाब का सिक्ख संप्रदाय और महाराष्ट्र के बारकरी संप्रदाय ने शूद्र महत्त्व धार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया। दसनामी नागा साधुओं के जूना, आवाहन, निरंजिनी, आनंद, महानिर्वाणी, अतल, जगन, अवलिया, सूखड़ और गूदड़-अखाड़ों में शूद्रप्रवेश हो सकता था।
सामाजिक स्थिति
वत्स कवष ऐलूष, कक्षीवान ओर सत्यकाम जाबाल की कथाओं से ज्ञात होता है कि शूद्र और द्विजों में उत्तर वैदिक काल में वैवाहिक संबंध हो जाया करता था यद्यपि यह सामान्यत: अच्छा नहीं माना गया होगा। वैश्य और शूद्रों में विवाह सामान्य रूप से प्रचलित था।[51]
बौद्ध
भद्दसालजातक और वासवखत्तिया के पुत्रविडुदभ की कथाओं से ज्ञात होता है कि बौद्ध समाज में अन्नपान और विवाह के संबंध में जातिगत वैषम्य था किंतु बौद्ध संघ में यह विभेद स्वीकार नहीं था। सुत्तनिपात के आमगंधसूत्र में बुद्ध का स्पष्ट कथन है कि किसी के द्वारा भी बनाए गए भोजन से अशौच नहीं होता। महापरिनिब्बान के ठीक पहले बुद्ध ने कुम्भार पुत्र चुंडा के यहाँ सुवकमादव ग्रहण किया था। श्रावस्ती के मालाकार जेट्ठक की धीता ही मल्लिका थी जो उदयन के साथ विवाहित हुई। काष्ठहारी की पुत्री[52] और फलविक्रेता की कन्या[53] अग्गमहिषी बन सकती थी। ललितविस्तार और वज्रसूत्री में प्रतिनिधि बौद्ध मत उल्लिखित है कि शूद्रा से विवाह पातक का कारण नहीं।
जैन
'शूद्र भोजन शुश्रुषा नरकाय भवेदिदम्'[54] प्रतिनिधि जैन मत है। किंतु साधुओं को ऊँच नीच के भेद करने का निषेध था।[55] इसी प्रकार 'शूद्रा शूद्रेण' वोढव्य नान्या[56] विवाह का प्रचलित विचार था, किंतु शूद्राओं का उच्च वर्ण में संभवत: विवाह होता था। मालाकार की पुत्री बनी हुई पद्मावती से राजा दंतीवाहन का विवाह करकंड महाराज कथानक वृहत्कथा कोष[57] में वर्णित है।
धर्मसूत्र स्मृति
पद से उत्पन्न होने के कारण पदपरिचर्या शूद्रों का विशिष्ट व्यवसाय है। द्विजों के साथ आसन, शयन वाक और पथ में समता की इच्छा रखने वाला शूद्र दंड्य है।[58] द्विजों के प्रति आक्रोश करने पर शूद्र को शारीरिक दंड दिया जा सकता है। कम उम्र का आर्य वृद्ध शूद्र से भी प्रणाम का अधिकारी है। शूद्र के साथ ब्राह्मण का विवाह निषिद्ध और अन्य द्विजों का अप्रशस्त है।[59] मनु के अनुसार शूद्रों को आसुर विवाह पद्धति विशेष रूप से विहित है।[60]
राजनीतिक स्थिति
तैत्तरीय संहिता में राज्याभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जन्य (शूद्र) क्रमश: पर्ण, औदुंबर, अश्वत्थ और निग्रोध के घट से राजा का अभिषेक करते हैं। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में[61] 'मान्यशूद्र' आमंत्रित थे। विराट की 'मंत्रिसभा' 'विप्र राजन्य विशसशूद्रका' थी।[62] भीष्म का अनुशासन है कि राजा की मंत्रिसभा में चार प्रगल्भ सात्विक ब्राह्मण, दस अथवा आठ शस्त्रपाणि क्षत्रिय, 21 संपन्न वैश्य और 3 विनीत शूद्र हों।[63] पश्चिमोत्तर में आभीर और निषादों के प्रतिवेश में शूद्रों का संभवत: एक गणराज्य भी था।[64] मनु[65] डायोडोरस, टॉल्मी, ह्वेनसांग[66] शूद्र राज्य का उल्लेख करते हैं।[67] के अनुसार 'सौराष्ट्र अवंति-शूद्र-अर्बुद-मरुभूमि' पर व्रात्य द्विज, आभीर और शूद्र शासन करेंगे। मृच्छकटिक का अंत ही शूद्रराज के अभिषेक से होता है। मुद्राओं तथा अभिलेखों से अनेक शूद्र राजाओं तथा राज्याधिकारों का पता मिलता है।
आर्थिक स्थिति
उत्तर वैदिक काल में शूद्र की स्थिति दास अथवा सर्फ की थी (वैदिक इंडेक्स) अथवा नहीं,[68] इस विषय में निश्चित नहीं कहा जा सकता। वह कर्मकर और परिचर्या करने वाला वर्ग था। सर्वमेघ, अश्वमेध और एकाह के अवसर पर 'भूमिशूद्रवर्ज्य' दान के नियम से यह अनुमित किया जा सकता है कि शूद्र के ऊपर स्वामित्त्व नहीं माना जाता था।
- बौद्ध वाङ्मय
बौद्ध वाङ्मय में वड्ठकी, कंभार (लोहार), चम्मकार, चित्तकार[69] आदि की श्रेणियों का उल्लेख है। इनके 'जेट्ठक' और 'पमुस' रहा करते थे।
- जैन वाङ्मय
बौद्ध साहित्य की 'हीन जाति' और 'हीन सिप्प' समान ही जैन वाङ्मय में 'आर्य सिप्प' और 'अनार्य सिप्प' का भेद है। आर्यशिल्प में दर्जी, तंतुवाय, छत्रकार इत्यादि तथा अनार्य शिल्पियों में चमार, नाई की गिनती थी।
व्यवहारगत
धर्मसूत्र, अर्थशास्त्र और स्मृतियों से शूद्र संबंधी व्यवहार ज्ञात होता है। सामाजिक वैषम्य के कारण सामान्यत: चतुर्वर्णपरक दंडसमता प्रचलित नहीं थी। वाक्पारुष्य और स्त्रीसंग्रहण में समान अपराधों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र के लिए विभिन्न दंडों का विधान था।[70]
इन्हें भी देखें: हिन्दू धर्म, वर्ण व्यवस्था, जाति, जाट, कायस्थ, वैश्य, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय
|
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- विधुशेखर भट्टाचार्य : 'दि स्टेट्स ऑव् शूद्राज़ इन एन्शिएन्ट इंडिया', विश्वभारती त्रैमासिक 1924 तथा शूद्र, इंडियन एंटीक्वेरी 1951
- रामशरण शर्मा : 'स्टडीज़ इन एन्शिएन्ट इंडिया, दिल्ली 1958
- बी.आर. अंबेडकर : 'हू वर दि शूद्राज', बंबई, 1946
- आल्फ्रडे हिल्लेब्रांट : 'ब्राह्मण शूद्राज़', ब्रेसलाउ 1896
पाठक, विशुद्धानंद “खण्ड 11”, हिन्दी विश्वकोश, 1969 (हिन्दी), भारतडिस्कवरी पुस्तकालय: नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी, 291-293।
- ↑ वेदांतसूत्र- 1, 44, 33
- ↑ अथर्ववेद 19, 32, 8
- ↑ रामशरण शर्मा पृ. 163-164
- ↑ गौतम धर्मसूत्र 12, 5
- ↑ वायुपुराण 1, 8, 158
- ↑ वेदांतसूत्र 1, 3, 34
- ↑ वेदांतसूत्र- 1, 44, 33
- ↑ वेदांतसूत्र- 3, 95
- ↑ वाकरनागेल, द्रष्टव्य रामशरण शर्मा, पृ. 35
- ↑ ऋग्वेद 10, 92, 2
- ↑ पंचविंश ब्राह्मण 5, 1, 6-10
- ↑ वाजसनेयी संहिता 31, 11
- ↑ महाभारत 12, 73, 4-8
- ↑ वायु पुराण1, 8, 155-59, विष्णु पुराण1, 6, धर्मसूत्र- वसिष्ठ धर्म सूत्र 4, 2, स्मृतियों में (मनु,, 1, 31) शुद्ध अथवा समिश्र रूप से प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों (शतपथ ब्राह्मण 14, 4, 2, 23, बृहदारण्यक 1, 4, 11
- ↑ वायुपुराण 9, 194-195, विष्णु 1, 6, 5-6 भी
- ↑ दीघनि. 1,90 और 100
- ↑ आचाराम सूत्रचूर्णि 4, 5, 6 आदिपुराण, 16, 148
- ↑ हत्वादस्यून् प्र आर्य वर्ण मावत्
- ↑ प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्रार्याय
- ↑ अर्थात् 19, 32, 8 वाजसनेयी संहिता में
- ↑ 2।4।10
- ↑ 4।3।93
- ↑ महाभारत वनपर्व, 297।60
- ↑ पाणिनीकालीन भारत |लेखक: वासुदेवशरण अग्रवाल |प्रकाशक: चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-1 |संकलन: भारतकोश पुस्तकालय |पृष्ठ संख्या: 92-93 |
- ↑ वाजस. सं. 30, 5
- ↑ काठक सं. 30, 7, 1
- ↑ ऐतरेय ब्राह्मण 7, 294
- ↑ अथर्ववेद 19, 32, 8
- ↑ बृहद्देवता 4, 25-26
- ↑ पंचविंश ब्राह्मण 14, 11, 17
- ↑ पंचविंश 14, 6, 6
- ↑ ऋग्वेद 10, 30, 34
- ↑ गौतमधर्मसूत्र 12, 4
- ↑ अश्वघोष की वज्रसूची पृष्ठ 5
- ↑ उत्राध्ययन सूत्र 12, 1, 2
- ↑ उवासगदसाओ पृ. 204
- ↑ नीतिकाव्यामृत 8, 12
- ↑ प्रवचनसार 3, यशस्तिलक 8, 43
- ↑ धर्मसंग्रह श्रावकाचार्य 9, 145-146
- ↑ कुलार्णव तंत्र, 8, 96
- ↑ कुलार्णव तंत्र- 4, 67, 75
- ↑ परमसंहिता, 17, 13-14
- ↑ जयाख्य 15, 187-88
- ↑ परमसंहिता 17, 4
- ↑ सात्वत 19, 53-54
- ↑ स्कंद, वैष्णव, मार्गशीर्ष माहात्म्य 2, 21-29
- ↑ देवी भागवत 12, 7, 10
- ↑ शांतिपर्व 60, 38
- ↑ शांतिपर्व 60, 38
- ↑ नस, उत्तरकांड
- ↑ तैत्तरीय सं. 7, 4, 19, 3
- ↑ कट्टहार जातक
- ↑ जातक 3, 14
- ↑ बृहत्कथा कोष 30, 13
- ↑ उवासगदसाओ पृ. 181-84
- ↑ आदिपुराण 26, 247
- ↑ वृहत्कथा कोष 145-147
- ↑ गौतम धर्मसूत्र 12, 5
- ↑ मनु. 3, 16, 19
- ↑ मनु. 3, 24
- ↑ महाभारत 14, 90, 24-35
- ↑ विराट 9, 25
- ↑ शांतिपर्व, महाभारत, 86, 7-9
- ↑ सभा. 29, 8-9
- ↑ मनु 4, 61
- ↑ वाटर्स, 2 पृ. 252
- ↑ विष्णुपुराण 4, 25, 18
- ↑ रामशरण शर्मा पृ. 163-164
- ↑ जातक 6, पृ. 22 और 427
- ↑ गौतम, धर्मसूत्र 12, 1
