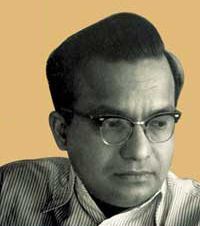"जगदीशचन्द्र माथुर": अवतरणों में अंतर
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
| पंक्ति 49: | पंक्ति 49: | ||
* जिन्होंने जीना जाना (1972 ई.) | * जिन्होंने जीना जाना (1972 ई.) | ||
==साहित्यिक विशेषताएँ== | ==साहित्यिक विशेषताएँ== | ||
जगदीशचन्द्र माथुर जी के प्रारंभिक नाटकों में कौतूहल और स्वच्छंद प्रेमाकुलता है। 'भोर का तारा' में कवि शेखर की भावुकता पर्यावरण में घटित करने या रचने का मोह भी प्रारंभ से मिलता है। परंतु समसामयिक को अनुभव के रूप में अनुभूत करके उसकी प्रामाणिकता को संस्कृति के माध्यम से सिद्ध करने का जो आग्रह उनके नाटकों में हैं उसकी रचनात्मक संभावना का प्रमाण 'कोणार्क' में है। परंपरा को माध्यम और संदर्भ के रूप में प्रयोग करने की कला में माथुर सिद्दहस्त हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि यही उनका सब कुछ है, बल्कि उन्होंने''' रीढ़ की हड्डी''' आदि ऐसे नाटक भी लिखे जिनका संबंध समाज के भीतर के बदलते रिश्तों और मानवीय संबंधों से है। 'शारदीया' के सारे नाटकों में समस्या को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का आभास अवश्य है, परंतु समस्या मात्र का परिवृत्त इतना छोटा है कि वह किसी व्यापक सत्य का आधार नहीं बन पाती। वस्तुतः माथुर छायावादी संवेदना के रचनाकार हैं। यह संवेदना 'भोर का तारा' से लेकर 'पहला राजा' तक में कमोबेश मिलती है। यह अवश्य है कि यह छायावादिता नाटक के विधागक संस्कार और यथार्थ के प्रति गहरी संसक्ति के कारण 'कोणार्क' और 'पहला राजा' में काफ़ी संस्कारित हुई है। | जगदीशचन्द्र माथुर जी के प्रारंभिक नाटकों में कौतूहल और स्वच्छंद प्रेमाकुलता है। 'भोर का तारा' में कवि शेखर की भावुकता पर्यावरण में घटित करने या रचने का मोह भी प्रारंभ से मिलता है। परंतु समसामयिक को अनुभव के रूप में अनुभूत करके उसकी प्रामाणिकता को संस्कृति के माध्यम से सिद्ध करने का जो आग्रह उनके नाटकों में हैं उसकी रचनात्मक संभावना का प्रमाण 'कोणार्क' में है। परंपरा को माध्यम और संदर्भ के रूप में प्रयोग करने की कला में माथुर सिद्दहस्त हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि यही उनका सब कुछ है, बल्कि उन्होंने''' रीढ़ की हड्डी''' आदि ऐसे नाटक भी लिखे जिनका संबंध समाज के भीतर के बदलते रिश्तों और मानवीय संबंधों से है। 'शारदीया' के सारे नाटकों में समस्या को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का आभास अवश्य है, परंतु समस्या मात्र का परिवृत्त इतना छोटा है कि वह किसी व्यापक सत्य का आधार नहीं बन पाती। वस्तुतः माथुर छायावादी संवेदना के रचनाकार हैं। यह संवेदना 'भोर का तारा' से लेकर 'पहला राजा' तक में कमोबेश मिलती है। यह अवश्य है कि यह छायावादिता नाटक के विधागक संस्कार और यथार्थ के प्रति गहरी संसक्ति के कारण 'कोणार्क' और 'पहला राजा' में काफ़ी संस्कारित हुई है।{{दाँयाबक्सा|पाठ=सरकार किसी भी भाषा से चलाई जाए पर लोकतंत्र हिंदी और भारतीय भाषाओं के बल पर ही चलेगा|विचारक=जगदीशचन्द्र माथुर}} | ||
====समीक्षा==== | ====समीक्षा==== | ||
'कोणार्क' उत्तम नाटक है। इतिहास, संस्कृति और समकालीनता मिलकर निरवधिकाल की धारणा और मानवीय सत्य की आस्था को परिपुष्ट करते हैं। घटना की तथ्यता और नाटकीयता के बावजूद महाशिल्पी विशु की चिंता और धर्मपद का साहसपूर्ण प्रयोग, व्यवस्था की अधिनायकवादी प्रवृत्ति से लड़ने और जुझने की प्रक्रिया एवं उसकी परिणति का संकेत नाटक को महत्वपूर्ण रचना बना देता है। कल्पना की रचनात्मक सामर्थ्य और संस्कृति का समकालीन अनुभव कोणार्क की सफल नाट्य कृति का कारण है। कोणार्क के अंत और घटनात्मक तीव्रता तथा परिसमाप्ति पर विवाद संभव है, परंतु उसके संप्रेषणात्मक प्रभाव पर प्रश्न चिन्ह संभव नहीं है। 'पहला राजा' नाटक के रचना-विधान और वातावरण को 'माध्यम' और 'संदर्भ' में रूप में प्रयोग करके लेखक ने व्यवस्था और प्रजाहित के आपसी रिश्तों को मानवीय दृष्टि से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। स्पुतनिक, अपोलो आदि के प्रयोग के कारण समकालीनता का अहसास गहराता है। पृथु, उर्वी, कवष आदि का प्रयास और उसका परिणाम सब मिलकर नाटक की समकालीनता को बराबर बनाए रखते हैं। पृथ्वी की उर्वर शक्ति, पानी और फावड़ा-कुदाल आद् को उपयोग रचना के काल को स्थिर करता है। 'परंपराशील नाट्य' महत्वपूर्ण समीक्षा-कृति है। इसमें लोक नाट्य की परंपरा और उसकी सामर्थ्य के विवेचन के अलावा [[नाटक]] की मूल दृष्टि को समझाने का प्रयास किया गया है। [[रामलीला]], [[रासलीला]] आदि से संबद्ध नाटकों और उनकी उपादेयता के संदर्भ में परंपरा का समकालीन संदर्भ में महत्व और उसके उपयोग की संभावना भी विवेच्य है। 'दस तसवीरें' और 'इन्होंने जीना जाना है' रचनाकार के मानस पर प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों की तस्वीरें और जीवनियाँ हैं, जिनका महत्व उनके रेखांकन और प्रभावांकन की दृष्टि से अक्षुण्ण है।<ref name="ज्ञानमण्डल">{{cite book | last =वर्मा | first =डॉ. धीरेंद्र | title =हिन्दी साहित्य कोश-2 | edition = | publisher =ज्ञानमण्डल लिमिटेड, [[वाराणसी]]| location =भारतडिस्कवरी पुस्तकालय | language = हिन्दी | pages =198 | chapter =}}</ref> | 'कोणार्क' उत्तम नाटक है। इतिहास, संस्कृति और समकालीनता मिलकर निरवधिकाल की धारणा और मानवीय सत्य की आस्था को परिपुष्ट करते हैं। घटना की तथ्यता और नाटकीयता के बावजूद महाशिल्पी विशु की चिंता और धर्मपद का साहसपूर्ण प्रयोग, व्यवस्था की अधिनायकवादी प्रवृत्ति से लड़ने और जुझने की प्रक्रिया एवं उसकी परिणति का संकेत नाटक को महत्वपूर्ण रचना बना देता है। कल्पना की रचनात्मक सामर्थ्य और संस्कृति का समकालीन अनुभव कोणार्क की सफल नाट्य कृति का कारण है। कोणार्क के अंत और घटनात्मक तीव्रता तथा परिसमाप्ति पर विवाद संभव है, परंतु उसके संप्रेषणात्मक प्रभाव पर प्रश्न चिन्ह संभव नहीं है। 'पहला राजा' नाटक के रचना-विधान और वातावरण को 'माध्यम' और 'संदर्भ' में रूप में प्रयोग करके लेखक ने व्यवस्था और प्रजाहित के आपसी रिश्तों को मानवीय दृष्टि से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। स्पुतनिक, अपोलो आदि के प्रयोग के कारण समकालीनता का अहसास गहराता है। पृथु, उर्वी, कवष आदि का प्रयास और उसका परिणाम सब मिलकर नाटक की समकालीनता को बराबर बनाए रखते हैं। पृथ्वी की उर्वर शक्ति, पानी और फावड़ा-कुदाल आद् को उपयोग रचना के काल को स्थिर करता है। 'परंपराशील नाट्य' महत्वपूर्ण समीक्षा-कृति है। इसमें लोक नाट्य की परंपरा और उसकी सामर्थ्य के विवेचन के अलावा [[नाटक]] की मूल दृष्टि को समझाने का प्रयास किया गया है। [[रामलीला]], [[रासलीला]] आदि से संबद्ध नाटकों और उनकी उपादेयता के संदर्भ में परंपरा का समकालीन संदर्भ में महत्व और उसके उपयोग की संभावना भी विवेच्य है। 'दस तसवीरें' और 'इन्होंने जीना जाना है' रचनाकार के मानस पर प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों की तस्वीरें और जीवनियाँ हैं, जिनका महत्व उनके रेखांकन और प्रभावांकन की दृष्टि से अक्षुण्ण है।<ref name="ज्ञानमण्डल">{{cite book | last =वर्मा | first =डॉ. धीरेंद्र | title =हिन्दी साहित्य कोश-2 | edition = | publisher =ज्ञानमण्डल लिमिटेड, [[वाराणसी]]| location =भारतडिस्कवरी पुस्तकालय | language = हिन्दी | pages =198 | chapter =}}</ref> | ||
==सूचना संचार क्राँति के जनक== | ==सूचना संचार क्राँति के जनक== | ||
{{दाँयाबक्सा|पाठ=दूरदर्शन जैसे माध्यम की शक्ति को पहचानिए और जैसा कि पश्चिम के मीडिया पंडित कहते हैं, ‘मीडिया इज़ द मौसेज’ इस भ्रम को तोड़िए और साबित कीजिए कि ‘मैन बिहाइंड मीडिया इज़ द मैसेज’|विचारक=जगदीशचंद्र माथुर}} | |||
जगदीशचंद्र माथुर को याद करना, सूचना संचार माध्यमों में हुई क्राँति को याद करना है। उनकी स्मृति को लेकर [[राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय]], [[दिल्ली]] ने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। इसकी वजह थी कि जगदीशचंद्र माथुर [[हिंदी]] के बहुत महत्वपूर्ण नाटककार थे। यों तो [[जयशंकर प्रसाद]] के बाद नाटक लेखन के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण मिश्र एक बड़ा नाम हैं पर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में प्रसाद की परंपरा से अलग हटकर प्रयोगशील नाटक लिखने की पहल जगदीशचंद्र माथुर ने अपने अप्रतिम नाटक ‘कोणार्क’ से की। वे एक सिद्धहस्त एकांकीकार भी थे। उनकी प्रयोगशीलता का सफल प्रमाण यही है कि उनके सम्पूर्ण नाटक ‘कोणार्क’ में एक भी नारी पात्र नहीं है लेकिन फिर भी वह बेहद सफलतापूर्वक मंचित होकर दर्शकों का चहेता मंच नाटक बना रहा है। और आज भी वह कई संदर्भों में चर्चा का केंद्र बना रहता है। यह मामूली बात नहीं है क्योंकि ‘कोणार्क’ नाटक की रचना आज से लगभग छह दशक पहले हुई थी। | जगदीशचंद्र माथुर को याद करना, सूचना संचार माध्यमों में हुई क्राँति को याद करना है। उनकी स्मृति को लेकर [[राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय]], [[दिल्ली]] ने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। इसकी वजह थी कि जगदीशचंद्र माथुर [[हिंदी]] के बहुत महत्वपूर्ण नाटककार थे। यों तो [[जयशंकर प्रसाद]] के बाद नाटक लेखन के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण मिश्र एक बड़ा नाम हैं पर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में प्रसाद की परंपरा से अलग हटकर प्रयोगशील नाटक लिखने की पहल जगदीशचंद्र माथुर ने अपने अप्रतिम नाटक ‘कोणार्क’ से की। वे एक सिद्धहस्त एकांकीकार भी थे। उनकी प्रयोगशीलता का सफल प्रमाण यही है कि उनके सम्पूर्ण नाटक ‘कोणार्क’ में एक भी नारी पात्र नहीं है लेकिन फिर भी वह बेहद सफलतापूर्वक मंचित होकर दर्शकों का चहेता मंच नाटक बना रहा है। और आज भी वह कई संदर्भों में चर्चा का केंद्र बना रहता है। यह मामूली बात नहीं है क्योंकि ‘कोणार्क’ नाटक की रचना आज से लगभग छह दशक पहले हुई थी। | ||
====एआईआर से आकाशवाणी तक==== | ====एआईआर से आकाशवाणी तक==== | ||
11:54, 29 दिसम्बर 2014 का अवतरण
जगदीशचन्द्र माथुर
| |
| पूरा नाम | जगदीशचन्द्र माथुर |
| जन्म | 16 जुलाई, 1917 |
| जन्म भूमि | खुर्जा, बुलंदशहर ज़िला, उत्तर प्रदेश |
| मृत्यु | 14 मई, 1978 |
| कर्म-क्षेत्र | नाटककार एवं लेखक |
| मुख्य रचनाएँ | कोणार्क, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, पहला राजा, शारदीया आदि |
| भाषा | हिन्दी |
| विद्यालय | प्रयाग विश्वविद्यालय |
| शिक्षा | एम.ए. |
| नागरिकता | भारतीय |
| अन्य जानकारी | परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक समय में जगदीशचंद्र माथुर, आईसीएस, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ही 'एआईआर' का नामकरण आकाशवाणी किया था। |
| इन्हें भी देखें | कवि सूची, साहित्यकार सूची |
जगदीशचन्द्र माथुर (अंग्रेज़ी: Jagdish Chandra Mathur, जन्म:16 जुलाई, 1917 - मृत्यु: 14 मई, 1978) हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिन्दी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। टेलीविज़न उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था। हिन्दी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वे ही रेडियो में लेकर आए थे। सुमित्रानंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह 'दिनकर' और बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया था।[1]
जीवन परिचय
जगदीशचन्द्र माथुर का जन्म 16 जुलाई, 1917 ई. खुर्जा, बुलंदशहर ज़िला, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में हुई। उच्च शिक्षा युइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण औऱ प्रयाग के साहित्यिक संस्कार रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हैं। 1939 ई. में प्रयाग विश्वविद्यालय से एम.ए. (अंग्रेज़ी) करने के बाद 1941 ई. में 'इंडियन सिविल सर्विस' में चुन लिए गए।[2]
कार्यक्षेत्र
सरकारी नौकरी में 6 वर्ष बिहार शासन के शिक्षा सचिव के रूप में, 1955 से 1962 ई. तक आकाशवाणी- भारत सरकार के महासंचालक के रूप में, 1963 से 1964 ई. तक उत्तर बिहार (तिरहुत) के कमिश्नर के रूप में कार्य करने के बाद 1963-64 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में विज़िटिंग फेलो नियुक्त होकर विदेश चले गए। वहाँ से लौटने के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए 19 दिसम्बर 1971 ई. से भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। इन सरकारी नौकरियों में व्यस्त रहते हुए भी भारतीय इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित करने का प्रयास चलता ही रहा।[2]
साहित्यिक परिचय
अध्ययनकाल से ही उनका लेखन प्रारंभ होता है। 1930 ई. में तीन छोटे नाटकों के माध्यम से वे अपनी सृजनशीलता की धारा के प्रति उन्मुख हुए। प्रयाग में उनके नाटक 'चाँद', 'रुपाभ' पत्रिकाओं में न केवल छपे ही, बल्कि इन्होंने 'वीर अभिमन्यु', आदि नाटकों में भाग लिया। 'भोर का तारा' में संग्रहीत सारी रचनाएँ प्रयाग में ही लिखी गईं। यह नाम प्रतीक रूप में शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों से जगदीशचन्द्र माथुर के रचनात्मक व्यक्तित्व के 'भोर का तारा' ही है। इसके बाद की रचनाओं में समकालीनता और परंपरा के प्रति गहराई क्रमशः बढ़ती गई है। व्यक्तियों, घटनाओं और देशके विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त अनुभवों ने सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।[2]
मुख्य कृतियाँ
- भोर का तारा (1946 ई.),
- कोणार्क (1950 ई.),
- ओ मेरे सपने (1950 ई.)
- शारदीया (1959 ईं),
- दस तस्वीरें (1962 ई.), '
- परंपराशील नाट्य (1968 ई.),
- पहला राजा (1970 ई.)
- जिन्होंने जीना जाना (1972 ई.)
साहित्यिक विशेषताएँ
जगदीशचन्द्र माथुर जी के प्रारंभिक नाटकों में कौतूहल और स्वच्छंद प्रेमाकुलता है। 'भोर का तारा' में कवि शेखर की भावुकता पर्यावरण में घटित करने या रचने का मोह भी प्रारंभ से मिलता है। परंतु समसामयिक को अनुभव के रूप में अनुभूत करके उसकी प्रामाणिकता को संस्कृति के माध्यम से सिद्ध करने का जो आग्रह उनके नाटकों में हैं उसकी रचनात्मक संभावना का प्रमाण 'कोणार्क' में है। परंपरा को माध्यम और संदर्भ के रूप में प्रयोग करने की कला में माथुर सिद्दहस्त हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि यही उनका सब कुछ है, बल्कि उन्होंने रीढ़ की हड्डी आदि ऐसे नाटक भी लिखे जिनका संबंध समाज के भीतर के बदलते रिश्तों और मानवीय संबंधों से है। 'शारदीया' के सारे नाटकों में समस्या को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का आभास अवश्य है, परंतु समस्या मात्र का परिवृत्त इतना छोटा है कि वह किसी व्यापक सत्य का आधार नहीं बन पाती। वस्तुतः माथुर छायावादी संवेदना के रचनाकार हैं। यह संवेदना 'भोर का तारा' से लेकर 'पहला राजा' तक में कमोबेश मिलती है। यह अवश्य है कि यह छायावादिता नाटक के विधागक संस्कार और यथार्थ के प्रति गहरी संसक्ति के कारण 'कोणार्क' और 'पहला राजा' में काफ़ी संस्कारित हुई है।
|
- जगदीशचन्द्र माथुर
|
समीक्षा
'कोणार्क' उत्तम नाटक है। इतिहास, संस्कृति और समकालीनता मिलकर निरवधिकाल की धारणा और मानवीय सत्य की आस्था को परिपुष्ट करते हैं। घटना की तथ्यता और नाटकीयता के बावजूद महाशिल्पी विशु की चिंता और धर्मपद का साहसपूर्ण प्रयोग, व्यवस्था की अधिनायकवादी प्रवृत्ति से लड़ने और जुझने की प्रक्रिया एवं उसकी परिणति का संकेत नाटक को महत्वपूर्ण रचना बना देता है। कल्पना की रचनात्मक सामर्थ्य और संस्कृति का समकालीन अनुभव कोणार्क की सफल नाट्य कृति का कारण है। कोणार्क के अंत और घटनात्मक तीव्रता तथा परिसमाप्ति पर विवाद संभव है, परंतु उसके संप्रेषणात्मक प्रभाव पर प्रश्न चिन्ह संभव नहीं है। 'पहला राजा' नाटक के रचना-विधान और वातावरण को 'माध्यम' और 'संदर्भ' में रूप में प्रयोग करके लेखक ने व्यवस्था और प्रजाहित के आपसी रिश्तों को मानवीय दृष्टि से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। स्पुतनिक, अपोलो आदि के प्रयोग के कारण समकालीनता का अहसास गहराता है। पृथु, उर्वी, कवष आदि का प्रयास और उसका परिणाम सब मिलकर नाटक की समकालीनता को बराबर बनाए रखते हैं। पृथ्वी की उर्वर शक्ति, पानी और फावड़ा-कुदाल आद् को उपयोग रचना के काल को स्थिर करता है। 'परंपराशील नाट्य' महत्वपूर्ण समीक्षा-कृति है। इसमें लोक नाट्य की परंपरा और उसकी सामर्थ्य के विवेचन के अलावा नाटक की मूल दृष्टि को समझाने का प्रयास किया गया है। रामलीला, रासलीला आदि से संबद्ध नाटकों और उनकी उपादेयता के संदर्भ में परंपरा का समकालीन संदर्भ में महत्व और उसके उपयोग की संभावना भी विवेच्य है। 'दस तसवीरें' और 'इन्होंने जीना जाना है' रचनाकार के मानस पर प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों की तस्वीरें और जीवनियाँ हैं, जिनका महत्व उनके रेखांकन और प्रभावांकन की दृष्टि से अक्षुण्ण है।[2]
सूचना संचार क्राँति के जनक
|
- जगदीशचंद्र माथुर
|
जगदीशचंद्र माथुर को याद करना, सूचना संचार माध्यमों में हुई क्राँति को याद करना है। उनकी स्मृति को लेकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली ने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। इसकी वजह थी कि जगदीशचंद्र माथुर हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण नाटककार थे। यों तो जयशंकर प्रसाद के बाद नाटक लेखन के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण मिश्र एक बड़ा नाम हैं पर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में प्रसाद की परंपरा से अलग हटकर प्रयोगशील नाटक लिखने की पहल जगदीशचंद्र माथुर ने अपने अप्रतिम नाटक ‘कोणार्क’ से की। वे एक सिद्धहस्त एकांकीकार भी थे। उनकी प्रयोगशीलता का सफल प्रमाण यही है कि उनके सम्पूर्ण नाटक ‘कोणार्क’ में एक भी नारी पात्र नहीं है लेकिन फिर भी वह बेहद सफलतापूर्वक मंचित होकर दर्शकों का चहेता मंच नाटक बना रहा है। और आज भी वह कई संदर्भों में चर्चा का केंद्र बना रहता है। यह मामूली बात नहीं है क्योंकि ‘कोणार्क’ नाटक की रचना आज से लगभग छह दशक पहले हुई थी।
एआईआर से आकाशवाणी तक
प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर के अनुसार जगदीशचंद्र माथुर एक साथ ही इंडियन सिविल सर्विस के वरिष्ठ प्रशासक, साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। ज़माना नेहरू जी का था। ग़ुलामी से मुक्त होकर देश ने आज़ादी की साँस ली थी। परिवर्तन और निर्माण का दौर था। अंग्रेज़ों की दासता की दो सदियों के बाद आज़ाद देश के भविष्य की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक संस्थानों को सांस्कृतिक सवालों को तब जल्द से जल्द तय किया जाना, सुलझाना और उनकी दिशाएँ सुनिश्चित करने का दायित्व सामने था। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के ऐसे ऐतिहासिक समय में जगदीशचंद्र माथुर, आईसीएस, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ही 'एआईआर' का नामकरण आकाशवाणी किया था।
दूरदर्शन की ताक़त
भारत में टेलीविज़न शुरू होने जा रहा था। माथुर साहब ने ही टीवी का नाम दूरदर्शन रखा था। दूरदर्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्घाटन के बाद स्टाफ मीटिंग में माथुर साहब ने कहा था, ‘‘सरकार किसी भी भाषा से चलाई जाए पर लोकतंत्र हिंदी और भारतीय भाषाओं के बल पर ही चलेगा।’’ "हिंदी ही सेतु का काम करेगी, सूचना और संचार तंत्र के सहारे ही हम अपनी निरक्षर जनता तक पहुँच सकते हैं। भारत के बहुमुखी विकास की क्राँति यहीं से शुरू होगी।" उन्होंने कहा था कि लोक संस्कृति के बिना शास्त्रीय कलाओं की शुचिता और सौंदर्य बाधित होगा। हमें एक क्षेत्र की लोक संस्कृति का अंतर्संबंध दूसरे क्षेत्र की लोक संस्कृति से स्थापित करना पड़ेगा। उन्होंने उस समय कहा था, "दूरदर्शन जैसे माध्यम की शक्ति को पहचानिए और जैसा कि पश्चिम के मीडिया पंडित कहते हैं, ‘मीडिया इज़ द मौसेज’ इस भ्रम को तोड़िए और साबित कीजिए कि ‘मैन बिहाइंड मीडिया इज़ द मैसेज’।"[1]
निधन
जगदीशचंद्र माथुर का निधन 14 मई, 1978 को हुआ।
|
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख